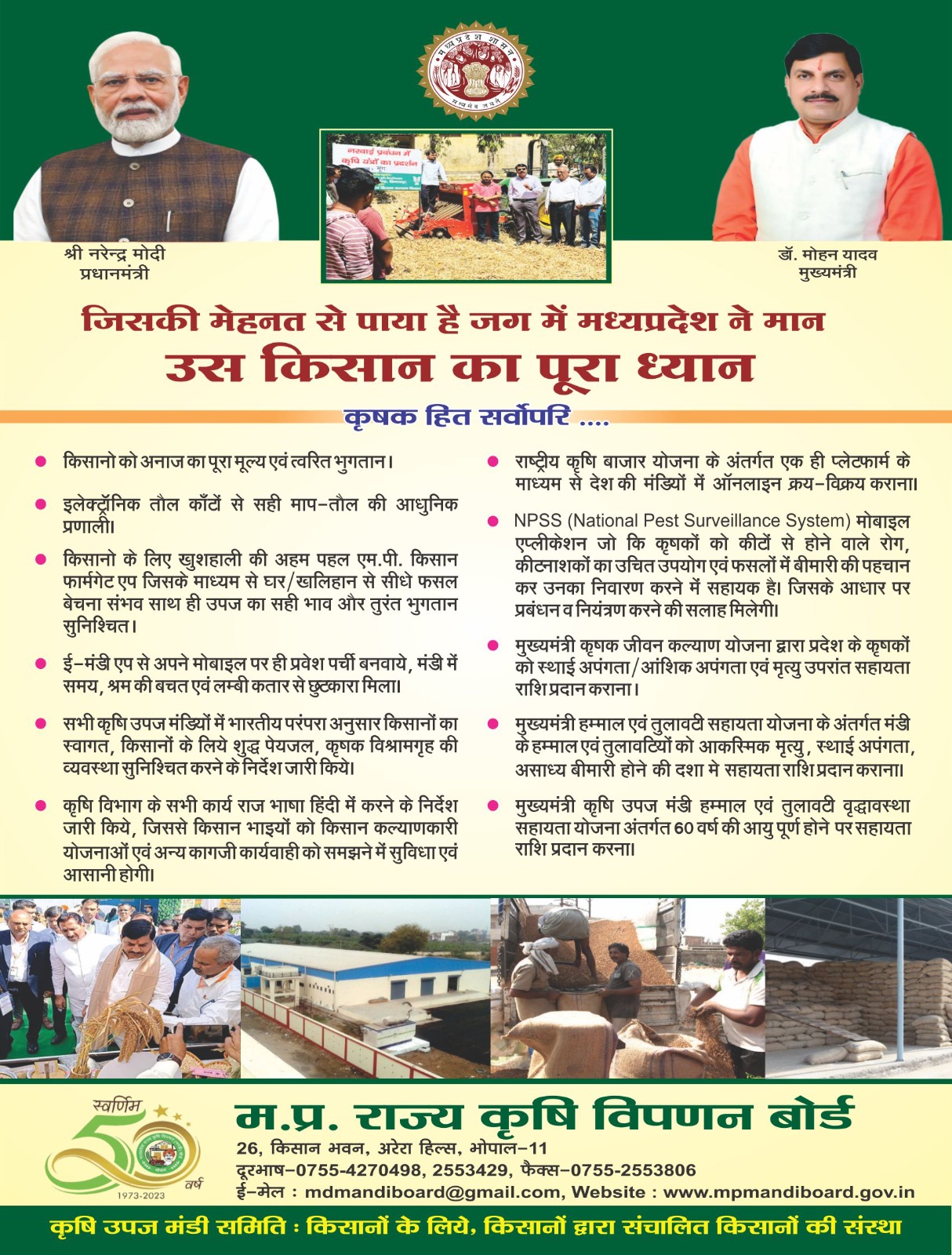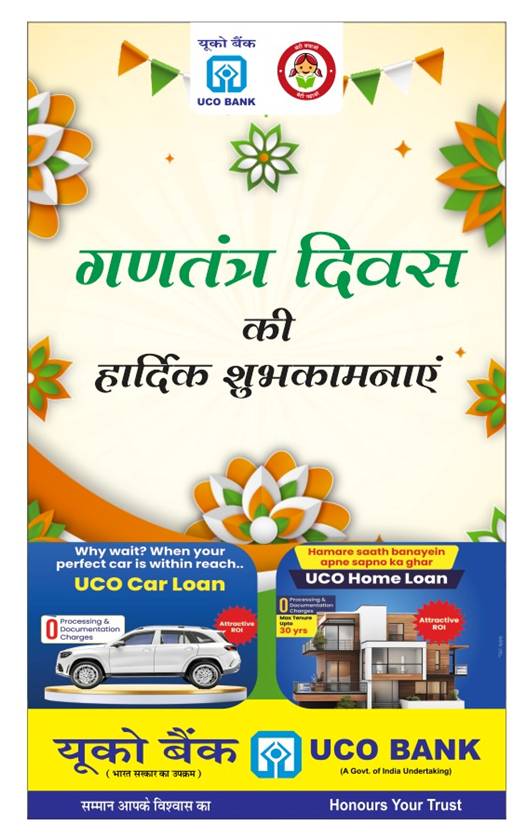डा. मुखर्जी के लिए राष्ट्रवाद ही पुरुषार्थ है

प्रखर राष्ट्रवादी और समता-समानता के पक्षधर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन (6 जुलाई) पर विशेष
-प्रहलाद सिंह पटेल-
राष्ट्रहित में पद-प्रतिष्ठा, सुख-सुविधाओं को त्यागने वाले महामानव कर्मयोगी डॉ. मुखर्जी के लिए मेरे आराध्य परमपूज्य श्रीश्री बाबाश्री की वाणी सामायिक है-'आदमियों के सोचने के ढंग भले एक हों, लेकिन विचारों के तरीके अलग-अलग होते हैं।'
21 अक्टूबर, 1951 को 'भारतीय जनसंघ' की स्थापना करने वाले डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और दूसरे आदमियों में यही मूल अंतर रहा। सोच कई प्रकार की हो सकती है। उदाहरण, एक 'विकसित भारत' की परिकल्पना और संकल्प की सोच समस्त राजनीतिक पार्टियों की एक समान हो सकती है, लेकिन 'वैचारिक दृष्टिकोण’ आवश्यक नहीं कि समान हों। मोदी सरकार जिस राष्ट्र के स्वप्न को साकार करने में पूर्ण प्रतिबद्धता से संलग्न है, उस वैचारिक दृष्टिकोण का आधार डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं।
उनके मंत्र-' एक निशान, एक प्रधान और एक विधान' को एक सोच नहीं; वैचारिक क्रांति के तौर पर देखा जाना चाहिए। नि:संदेह यह वाक्य तब विभाजन की पीड़ा भोग रहे और भारत से अलग-थलग पड़े 'जम्मू-कश्मीर' के संदर्भ में थी, लेकिन आज यह समग्र राष्ट्र के निए प्रासंगिक है। मोदी सरकार का ध्येय वाक्य-'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उसी विचार का 'परिष्कृत स्वरूप' अर्थात, 'उन्नत संस्करण' है। इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक समग्र राष्ट्र के विकास, अखंडता और समता-समानता का भाव है।
5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कड़े विरोध के बावजूद जम्मू-कश्मीर से 'अनुच्छेद 370' हटाने की घोषणा की, जो डॉ. मुखर्जी के 'अखंड भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक प्रयास था; एक कर्म था।
रामचरित मानस में एक चौपाई है-
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।
जो जस करहि सो तस फल चाखा॥
अर्थात, समस्त संसार कर्मों पर निर्भर है और हर व्यक्ति को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। डॉ. मुखर्जी ने सदैव कर्म को प्रधानता दी।
6 जुलाई, 1901 ये केवल एक तिथि नहीं है। यह भारत के भूत-वर्तमान और भविष्य को दिशा और गति देने वाले महान व्यक्तित्व, प्रखर राष्ट्रवादी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अवतरण का दिवस है। इन 124 सालों में भारत ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे; परंतु आज हम जिस पड़ाव पर हैं, वो इन्हीं महापुरुषों के निस्वार्थ कर्म और पुरुषार्थ का परिणाम है।
मुखर्जी के जीवन में 'पुरुषार्थ' सर्वोपरि रहा। देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने उन्होंने अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। हिंदू धर्म के प्राचीनतम पवित्र ग्रंथ; जिन्हें 'श्रुति' भी कहते हैं, यानी वेद शास्त्रों के अनुसार कर्म और पुरुषार्थ
भारतीय दर्शन और जीवनशैली के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है-मानव का उद्देश्य। बगैर कर्म के पुरुषार्थ मतलब; जीवन का लक्ष्य असंभावी है। डॉ. मुखर्जी का एक ही पुरुषार्थ रहा-'भारत में केवल एक विधान, एक प्रधान और एक निशान होना चाहिए।' यही राष्ट्रवाद है। अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना। यह तभी संभव है, जब समग्र देशवासी समता-समानता और एक झंडे तले एकता का परिचायक बनें।
पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है और जब उद्देश्य 'राष्ट्रवाद' से जुड़ा हो; तब 'त्याग' तपस्या बन जाता है। डॉ. मुखर्जी कलकत्ता(अब कोलकाता) के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और प्रख्यात शिक्षाविद थे।
अपने पिता के पदचिह्नों पर अग्रसर डॉ. मुखर्जी 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। 33 वर्ष की अल्पायु में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। वे सबसे कम उम्र के कुलपति थे। वे चाहते, तो सम्पूर्ण जीवन विलासितापूर्वक गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति की दुरूह राह चुनी। डॉ. मुखर्ची सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे।
ब्रिटिश सरकार द्वारा 'साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण' के कुत्सित प्रयासों के विरुद्ध उन्होंने अलख जगाने का कर्म किया। वे सदैव प्रयासरत रहे कि राष्ट्रहित के लिए, उसकी अखंडता के लिए एक ही विचारधारा रहे कि 'हम सब एक हैं' और यही आधारभूत सत्य है। 23 जून, 1953 को कश्मीर यात्रा के दौरान गिरफ्तारी और नजरबंदी के दौरान डॉ. मुखर्जी की रहस्यमयी मृत्यु इतिहास का वो काला धब्बा है, जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। 23 जून, 2018 को मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया था-'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि कोई भी राष्ट्र अपनी ही ऊर्जा से सुरक्षित रह सकता है।'
डॉ. मुखर्जी ने अपने पुरुषार्थ से इसी 'राष्ट्रवाद की ऊर्जा को जन-जन के भीतर पहुंचाया। एक ऐसी चेतना शक्ति; जो हमारे भीतर के 'स्व' से जाग्रत होती है। देश के 140 करोड़ भारतीयों में 'स्वयमेव मृगेन्द्रता' का भाव ऐसे ही विचारों का नतीजा है। यानी हर भारतीय स्वयं को श्रेष्ठ बनाने में जुट गया है। 'आत्मनिर्भर भारत' और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य उसी समय से शुरू हो गया था, तब डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 'राष्ट्रीय एकता' को सर्वोच्च पुरुषार्थ कहा था।
(लेखक मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री हैं।)