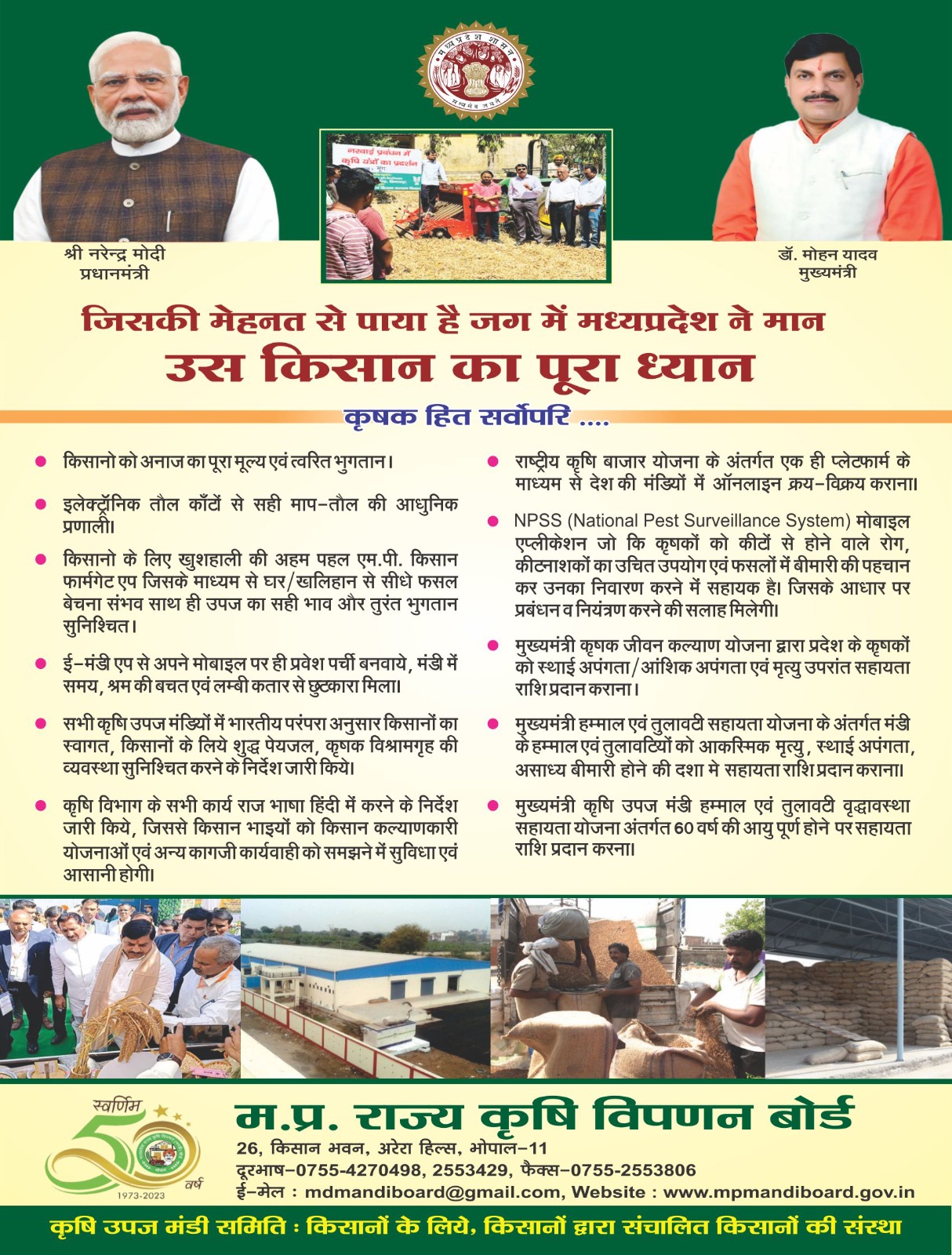लोकतंत्र को अब धर्म दंड की भी है आवश्यकता

दिव्य चिंतन
गुरु पूर्णिमा पर विशेष-
🖋 हरीश मिश्र
प्राचीन भारत की राजनैतिक व्यवस्था धर्मदंड और धर्मगुरुओं के आदेशों, दिशा-निर्देशों पर केंद्रित हुआ करती थी। इतिहास के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत में प्रारंभ से ही ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को विकसित करने के प्रयास हुए, जिससे सत्ता केवल सिंहासन पर बैठने का माध्यम न बन जाए। वह मात्र भोग-विलास की वस्तु न रह जाए। धर्मगुरुओं ने राजाओं को आर्थिक, धार्मिक और प्रजातांत्रिक अधिकार तो दिए, लेकिन सत्ता राजा-केंद्रित न हो, इसलिए धर्म के दंड को धर्मगुरु के आदेश के रूप में सर्वोच्च स्थान दिया गया।
जब-जब शासकों ने सत्ता के मद में चूर होकर मनमानी की, तब-तब इस देश की लोकतांत्रिक चेतना ने विद्रोह का बिगुल फूंका। कभी परशुराम ने फरसे से सत्ता में बैठे मदांध शासकों के सिर काट डाले, कभी श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र की सत्ता को उखाड़ फेंका। चाणक्य ने नंद वंश के अत्याचारी शासक धनानंद को उखाड़कर सत्ता की बागडोर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे योग्य शासक को सौंपी। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत की राजनैतिक व्यवस्था अपनी विशेषताओं के कारण सर्वोपरि रही।
प्राचीन व्यवस्था में राजा सर्वोच्च होता था, लेकिन वह धर्मगुरु की आज्ञा का पालन करता था। आज लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सर्वोच्च हैं, लेकिन अब धर्मगुरु का स्थान जनता और संविधान ने ले लिया है। दुखद यह है कि आज के जनप्रतिनिधियों को न तो संविधान का भय है, न ही जनता की चिंता।
ऋग्वेद में 'सभा' शब्द का आठ बार और अथर्ववेद में सत्रह बार उल्लेख मिलता है। उस काल में सभा की सदस्यता कठिन मानी जाती थी। सभासद वही बन सकता था जो यज्ञ—अर्थात् लोकोपयोगी कार्य करता हो।जो विद्वान, धर्मपालक, मृदुभाषी और चरित्रवान हो। आज की संसद और विधानसभाओं में बाहुबलियों, धनबलियों और भ्रष्टाचारियों की संख्या चिंता का विषय है।
भारत को एक बार फिर अपनी प्राचीन धर्मदंड-आधारित राजनैतिक व्यवस्था की ओर लौटना होगा। हमें अपनी राजनीति को फिर से सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से जोड़ना होगा। प्राचीन भारत की सत्ता "सत्यम शिवम सुंदरम" की ओर उन्मुख होती थी, जबकि आज की राजनीति भय, अपमान और लालच की त्रिवेणी बन गई है।
राजा दशरथ को वशिष्ठ जैसे धर्मगुरु का और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जैसे नीति पुरुष का मार्गदर्शन प्राप्त था। धर्मगुरु के मार्गदर्शन से सत्ता प्रजाहित एवं राष्ट्रहित की प्रेरणा लेती थी। किंतु जब से धर्मगुरुओं को सत्ता से पृथक किया गया, तब से नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ। राजनीति में प्रजावत्सलता समाप्त हो गई।
आज का राजनैतिक परिदृश्य अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता और असंवेदनशीलता से पीड़ित है। लोकतंत्र के मंदिरों—संसद व विधानसभाओं—में अब शालीन संवाद नहीं, बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, जिसे किसी भी स्थिति में गरिमामय नहीं कहा जा सकता।
हमें पुनः धर्मदंड और धर्मगुरु की शरण में जाना होगा। जब वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था धर्म और नीति से संचालित होगी, तभी भारत एक समृद्ध, नैतिक और सशक्त राष्ट्र बन सकेगा।
– लेखक : स्वतंत्र पत्रकार